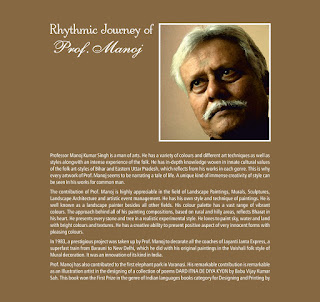मुल्ला और इंसाफ़
इधर बहुत दिनों से मुल्ला नसरुद्दीन की बड़ी याद आ रही है. मित्रों से निजी बातचीत के क्रम में उनका जिक्र भी अकसर होता रहा है. पढ़ता भी ख़ूब रहा हूं, गाहे-बगाहे जब भी मुल्ला के बारे में जो कुछ भी मिल गया. पर उधर जूते ने ऐसा परेशान कर रखा था कि मुल्ला को इयत्ता पर याद करने का मौक़ा ही नहीं मिल सका. आज एक ख़ास वजह से उनकी याद आई. एक बात आपसे पहले ही कर लूं कि मुल्ला से जुड़े इस वाक़ये को किसी अन्यथा अर्थ में न लें. कहा यह जाता है कि यह एक चुटकुला है, लिहाजा बेहतर होगा कि आप भी इसे एक चुटकुले के ही तौर पर लें. अगर किसी से इसका कोई साम्य हो जाता है तो उसे बस संयोग ही मानें. तो हुआ यह कि मुल्ला एक बार कहीं जा रहे थे, तब तक सज्जन दौड़ते-दौड़ते आए और उन्हें एक चाटा मार दिया. ज़ाहिर है, मुल्ला को बुरा लगना ही चाहिए था तो लगा भी. लेकिन इसके पहले कि मुल्ला उन्हें कुछ कहते, वह मुल्ला से माफ़ी मांगने लगे. उनका कहना था कि असल में उन्होंने मुल्ला को मुल्ला समझ कर तो चाटा मारा ही नहीं. हुआ यह कि मुल्ला को आते देख दूर से वह किसी और को समझ बैठे थे और इसी धोखे में उन्होंने चाटा मार दिया. पर मुल्ला तो मुल्ला ठहरे. उन